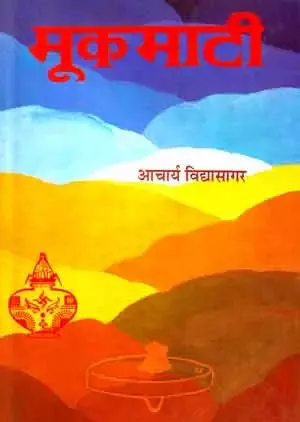|
जैन साहित्य >> मूक माटी मूक माटीआचार्य विद्यासागर
|
191 पाठक हैं |
|||||||
धर्म-दर्शन एवं अध्यात्म केसार को आज की भाषा एवं मुक्त-छन्द की मनोरम काव्य-शैली में निबद्ध कर कविता-रचना को नया आयाम देने वाली एक अनुपम कृति
Mook Maati
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
‘मूक माटी’ महाकाव्य का सृजन आधुनिक भारतीय साहित्य की एक उल्लेखनीय अपलब्धि है। यबसे पहली बात तो यह है कि माटी जैसी अकिंचिन, पद-दलित और तुच्छ वस्तु को महाकाव्य का विषय बनाने की कल्पना ही नितान्त अनोखी है। दूसरी बात यह कि माटी की तुच्छता के चरम भव्यता के दर्शन करके उसकी विशुद्धता और उपक्रम को मुक्ति की मंगल-यात्रा के रूपक में ढालना कविता के अध्यात्म के साथ अ-भेद की स्थिति में पहुँचना है। इसीलिए आचार्य श्री विद्यासागर की कृति ‘मूक माटी’ मात्र कवि कर्म नहीं है, यह एक दार्शनिक सन्त की आत्मा का संगीत है—सन्त जो साधना के जीवन्त प्रतिरूप हैं और साधना जो आत्म-विशुद्धि की मंज़िलों पर सावधानी से पग धरती हुई, लोक मंगल को साधती है। ये सन्त तपस्या से अर्जित जीवन-दर्शन को अनुभूति मे रचा-पचा कर सबके हृदय में गुंजरित कर देना चाहते हैं। निर्मल-वाणी और सार्थक सम्प्रेषण का जो योग इनके प्रवचनों में प्रस्फुटित होता है—उसमें मुक्ति छन्द का प्रवाह और काव्यानुभूति की अन्तरंग लय समन्वित करके आचार्यश्री ने इसे काव्य का रूप दिया है।
प्रारम्भ में ही य़ह प्रश्न उठना अप्रासंगिक न होगा कि ‘मूक माटी’ को महाकाव्य कहें या खण्ड-काव्य या मात्र काव्य। इसे महाकाव्य की परम्परागत परिभाषा के चौखटे में जड़ना सम्भव नहीं है, किन्तु यदि विचार करें कि चार खण्डों में विभाजित यह काव्य लगभग 500 पृष्ठों में समाहित है, तो परिणाम की दृष्टि से यह महाकाव्य की सीमाओं को छूता है। पहला पृष्ठ खोलते ही महाकाव्य के अनुरूप प्राकृतिक परिदृश्य मुखर हो जाता है :
सीमातीत शून्य में/नीलिमा बिछाई,
और....इधर नाचे/निरी नीरवता छाई।....
× × × × × ×
भानु की निद्रा टूट तो गई है
परन्तु अभी वह लेटा है/माँ की मार्दव-गोद में....
प्राची के अधरों पर/मन्द मधुरिम मुस्कान है....(पृष्ठ 1)
इसी सन्दर्भ में कुमुदिनी, कमलिनी, चाँद, तारे, सुगन्ध, पवन, सरिता-तट....और
सरिता-तट की माटी
अपना हृदय खोलती है/माँ धरती के सम्मुख। (पृष्ठ 4)
यह सारा प्राकृतिक परिदृश्य इस बिन्दु पर आकर एक मूलभूत दार्शनिक प्रश्न पर केन्द्रित हो जाता है :
इस पर्याय की/इति कब होगी ?....
बता दो, माँ...इसे !.....
कुछ उपाय करो माँ ! खुद अपाय हरो माँ !
और सुनो,/ विलम्ब मत करो
पद दो, पथ दो/पाथेय भी दो, माँ ! (पृष्ठ 5)
माटी की वेदना-व्यथा इससे पहले की बीस-तीस पक्तियों में इतनी तीव्रता और मार्मिकता से व्यक्त हुई है, कि करुणा साकार हो जाती है। माँ-बेटी का वार्तालाप क्षण-क्षण में सरिता की धारा के समान अचानक नया मोड़ ले जाता है और दार्शनिक चिन्तन मुखर हो जाता है। प्रत्येक तथ्य तत्त्व-दर्शन की उद्भावना में अपनी सार्थकता पाता है। ‘मूक माटी’ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पद्धति से जीवन-दर्शन परिभाषित हो जाता है । दूसरी बात यह कि यह दर्शन आरोपित नहीं लगता, अपने प्रसंग और परिवेश में से उद्धाटित होता है।
महाकाव्य की अपेक्षाओं के अनुरूप, प्राकृतिक परिवेश के अतिरिक्त, ‘मूक माटी’ में सृजन के अन्य पक्ष भी समाहित हैं। इस सन्दर्भ में सोचें तो प्रश्न होगा कि ‘मूक माटी ’ का नायक कौन है, नायिका कौन है ? बहुत ही रोचक प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर केवल अनेकान्त दृष्टि से ही सम्भव है। माटी तो नायिका है ही, कुम्भकार को नायक मान सकते हैं...किन्तु यह दृष्टि लौकिक अर्थ में घटित नहीं होती। यहाँ रोमांस आदि है तो आध्यात्मिक प्रकार का है। कितनी प्रतीक्षा रही है माटी को कुम्भकार की, युगों-युगों से, कि वह उद्धार करके अव्यक्त सत्ता में से घट की मंगल-मूर्ति उद्घाटित करेगा। मंगल-घट की सार्थकता गुरु के पाद-प्रक्षालन में है जो काव्य के पात्र, भक्त सेठ की श्रद्धा के आधार हैं।
शरण, चरण हैं आपके/तारण-तरण जहाज,
भव-दधि तट तक ले चलो/करुणाकर गुरुराज ! (पृष्ठ 325)
काव्य के नायक तो यही गुरु हैं किन्तु स्वयं गुरु के लिए अन्तिम नायक है अर्हन्त देव :
जो मोह से मुक्त हो जीते हैं
राग-रोष से रीते हैं
जनम-मरण-जरा-जीर्णता/ जिन्हें छू नहीं सकते अब...
सप्त भयों से मुक्त, अभय-निधान,
निद्रा-तन्द्रा जिन्हें घेरती नहीं ....
शोक से शून्य, सदा अशोक हैं।...
जिनके पास संग है न संघ,
जो एकाकी है,...
सदा-सर्वथा निश्चिन्त हैं,
अष्टादश दोषों से दूर। (पृष्ठ 326-327)
काव्य की दृष्टि से ‘मूक माटी’ में शब्दालंकार और अर्थालंकारों की छटा नये सन्दर्भों में मोहक है। कवि के लिए अतिशय आकर्षण है शब्द का, जिसका प्रचलित अर्थ में उपयोग करके वह उसकी संगठना को व्याकरण की सान पर चढ़ाकर नयी-नयी धरा देते हैं, नयी-नयी परतें उघाड़ते हैं। शब्द की व्युत्पत्ति उसके अन्तरंग अर्थ की झाँकी तो देती ही है, हमें उसके माध्यम से अर्थ के अनूठे और अछूते आयामों का दर्शन होता है। काव्य में से ऐसे कम-से-कम पचास उदाहरण एकत्र किये जा सकते हैं यदि हम कवि की अर्थान्वेषिणी दृष्टि ही नहीं उसके इस चमत्कार का भी ध्यान करें, जहाँ शब्द की ध्वनि अनेक साम्यों की प्रतिध्वनि में अर्थान्तरित होती है। उदाहरण को लिए :
युग के आदि में/इसका नामकरण हुआ है/कुम्भकार !
‘कु’ यानी धरती
और ‘भ’ यानी/ भाग्य होता है।
यहाँ पर जो/भाग्यवान् भाग्य-विधाता हो
कुम्भकार कहलाता है। (पृष्ठ 28)
भावना भाता हुआ गधा भगवान् से प्रार्थना करता है कि :
मेरा नाम सार्थक हो प्रभो !
यानी
‘गद’ का अर्थ है रोग
‘हा’ का अर्थ है हारक
मैं सबके रोगों का हन्ता बनूँ, ....बस। (पृष्ठ 40)
× × × × × × ×
राही बनना ही तो/ हीरा बनना है,
स्वयं राही शब्द ही/ विलोम-रूप से कह रहा है—
रा.....ही....ही.....रा
× × × ×
तन और मन को / तप की आग में/ तपा-तपा कर
जला-जला कर/ राख करना होगा...
तभी नहीं चेतन-आत्मा खरा उतरेगा।
खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है—
राख बने बिना/ खरा दर्शन कहाँ ?
रा...ख...ख...रा (पृष्ठ 57)
इसी प्रकार की शब्द-साधना से आन्तरिक अर्थ प्रकट हुए हैं—नारी, सुता, दुहिता, कुमारी, स्त्री, अबला आदि के।
यहाँ इंगित किया जा सकता है कि आचार्य-कवि की महिलाओं के प्रति आदर और आस्था के भाव प्रकट किये हैं। उनके शान्त, संयत रूप की शालीनता को सराहा है
‘मूक माटी’ मे कविता का अन्तरंग स्वरूप प्रतिबिम्बित है और साहित्य के आधारभूत सिद्धान्तों का दिग्दर्शन है। उद्धरण देने लगें तो कोई अन्त नहीं, क्योंकि वास्तव में काव्य का अधिकांश उद्धरणीय है जो कृति का उद्भुत गुण है। कवि की उक्ति है :
प्रारम्भ में ही य़ह प्रश्न उठना अप्रासंगिक न होगा कि ‘मूक माटी’ को महाकाव्य कहें या खण्ड-काव्य या मात्र काव्य। इसे महाकाव्य की परम्परागत परिभाषा के चौखटे में जड़ना सम्भव नहीं है, किन्तु यदि विचार करें कि चार खण्डों में विभाजित यह काव्य लगभग 500 पृष्ठों में समाहित है, तो परिणाम की दृष्टि से यह महाकाव्य की सीमाओं को छूता है। पहला पृष्ठ खोलते ही महाकाव्य के अनुरूप प्राकृतिक परिदृश्य मुखर हो जाता है :
सीमातीत शून्य में/नीलिमा बिछाई,
और....इधर नाचे/निरी नीरवता छाई।....
× × × × × ×
भानु की निद्रा टूट तो गई है
परन्तु अभी वह लेटा है/माँ की मार्दव-गोद में....
प्राची के अधरों पर/मन्द मधुरिम मुस्कान है....(पृष्ठ 1)
इसी सन्दर्भ में कुमुदिनी, कमलिनी, चाँद, तारे, सुगन्ध, पवन, सरिता-तट....और
सरिता-तट की माटी
अपना हृदय खोलती है/माँ धरती के सम्मुख। (पृष्ठ 4)
यह सारा प्राकृतिक परिदृश्य इस बिन्दु पर आकर एक मूलभूत दार्शनिक प्रश्न पर केन्द्रित हो जाता है :
इस पर्याय की/इति कब होगी ?....
बता दो, माँ...इसे !.....
कुछ उपाय करो माँ ! खुद अपाय हरो माँ !
और सुनो,/ विलम्ब मत करो
पद दो, पथ दो/पाथेय भी दो, माँ ! (पृष्ठ 5)
माटी की वेदना-व्यथा इससे पहले की बीस-तीस पक्तियों में इतनी तीव्रता और मार्मिकता से व्यक्त हुई है, कि करुणा साकार हो जाती है। माँ-बेटी का वार्तालाप क्षण-क्षण में सरिता की धारा के समान अचानक नया मोड़ ले जाता है और दार्शनिक चिन्तन मुखर हो जाता है। प्रत्येक तथ्य तत्त्व-दर्शन की उद्भावना में अपनी सार्थकता पाता है। ‘मूक माटी’ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पद्धति से जीवन-दर्शन परिभाषित हो जाता है । दूसरी बात यह कि यह दर्शन आरोपित नहीं लगता, अपने प्रसंग और परिवेश में से उद्धाटित होता है।
महाकाव्य की अपेक्षाओं के अनुरूप, प्राकृतिक परिवेश के अतिरिक्त, ‘मूक माटी’ में सृजन के अन्य पक्ष भी समाहित हैं। इस सन्दर्भ में सोचें तो प्रश्न होगा कि ‘मूक माटी ’ का नायक कौन है, नायिका कौन है ? बहुत ही रोचक प्रश्न है, क्योंकि इसका उत्तर केवल अनेकान्त दृष्टि से ही सम्भव है। माटी तो नायिका है ही, कुम्भकार को नायक मान सकते हैं...किन्तु यह दृष्टि लौकिक अर्थ में घटित नहीं होती। यहाँ रोमांस आदि है तो आध्यात्मिक प्रकार का है। कितनी प्रतीक्षा रही है माटी को कुम्भकार की, युगों-युगों से, कि वह उद्धार करके अव्यक्त सत्ता में से घट की मंगल-मूर्ति उद्घाटित करेगा। मंगल-घट की सार्थकता गुरु के पाद-प्रक्षालन में है जो काव्य के पात्र, भक्त सेठ की श्रद्धा के आधार हैं।
शरण, चरण हैं आपके/तारण-तरण जहाज,
भव-दधि तट तक ले चलो/करुणाकर गुरुराज ! (पृष्ठ 325)
काव्य के नायक तो यही गुरु हैं किन्तु स्वयं गुरु के लिए अन्तिम नायक है अर्हन्त देव :
जो मोह से मुक्त हो जीते हैं
राग-रोष से रीते हैं
जनम-मरण-जरा-जीर्णता/ जिन्हें छू नहीं सकते अब...
सप्त भयों से मुक्त, अभय-निधान,
निद्रा-तन्द्रा जिन्हें घेरती नहीं ....
शोक से शून्य, सदा अशोक हैं।...
जिनके पास संग है न संघ,
जो एकाकी है,...
सदा-सर्वथा निश्चिन्त हैं,
अष्टादश दोषों से दूर। (पृष्ठ 326-327)
काव्य की दृष्टि से ‘मूक माटी’ में शब्दालंकार और अर्थालंकारों की छटा नये सन्दर्भों में मोहक है। कवि के लिए अतिशय आकर्षण है शब्द का, जिसका प्रचलित अर्थ में उपयोग करके वह उसकी संगठना को व्याकरण की सान पर चढ़ाकर नयी-नयी धरा देते हैं, नयी-नयी परतें उघाड़ते हैं। शब्द की व्युत्पत्ति उसके अन्तरंग अर्थ की झाँकी तो देती ही है, हमें उसके माध्यम से अर्थ के अनूठे और अछूते आयामों का दर्शन होता है। काव्य में से ऐसे कम-से-कम पचास उदाहरण एकत्र किये जा सकते हैं यदि हम कवि की अर्थान्वेषिणी दृष्टि ही नहीं उसके इस चमत्कार का भी ध्यान करें, जहाँ शब्द की ध्वनि अनेक साम्यों की प्रतिध्वनि में अर्थान्तरित होती है। उदाहरण को लिए :
युग के आदि में/इसका नामकरण हुआ है/कुम्भकार !
‘कु’ यानी धरती
और ‘भ’ यानी/ भाग्य होता है।
यहाँ पर जो/भाग्यवान् भाग्य-विधाता हो
कुम्भकार कहलाता है। (पृष्ठ 28)
भावना भाता हुआ गधा भगवान् से प्रार्थना करता है कि :
मेरा नाम सार्थक हो प्रभो !
यानी
‘गद’ का अर्थ है रोग
‘हा’ का अर्थ है हारक
मैं सबके रोगों का हन्ता बनूँ, ....बस। (पृष्ठ 40)
× × × × × × ×
राही बनना ही तो/ हीरा बनना है,
स्वयं राही शब्द ही/ विलोम-रूप से कह रहा है—
रा.....ही....ही.....रा
× × × ×
तन और मन को / तप की आग में/ तपा-तपा कर
जला-जला कर/ राख करना होगा...
तभी नहीं चेतन-आत्मा खरा उतरेगा।
खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है—
राख बने बिना/ खरा दर्शन कहाँ ?
रा...ख...ख...रा (पृष्ठ 57)
इसी प्रकार की शब्द-साधना से आन्तरिक अर्थ प्रकट हुए हैं—नारी, सुता, दुहिता, कुमारी, स्त्री, अबला आदि के।
यहाँ इंगित किया जा सकता है कि आचार्य-कवि की महिलाओं के प्रति आदर और आस्था के भाव प्रकट किये हैं। उनके शान्त, संयत रूप की शालीनता को सराहा है
‘मूक माटी’ मे कविता का अन्तरंग स्वरूप प्रतिबिम्बित है और साहित्य के आधारभूत सिद्धान्तों का दिग्दर्शन है। उद्धरण देने लगें तो कोई अन्त नहीं, क्योंकि वास्तव में काव्य का अधिकांश उद्धरणीय है जो कृति का उद्भुत गुण है। कवि की उक्ति है :
शिल्पी के शिल्पक-साँचे में
साहित्य शब्द ढ़लता-सा !
‘‘हित से जो युक्त—समन्वित होता है
वह सहित माना है
और
सहित का भाव ही
साहित्य बाना है,
अर्थ यह हुआ कि
जिसके आवलोकन से
सुख का समुद्भव-सम्पादन हो
सही साहित्य वही है
अन्यथा,
सुरभि से विरहित पुष्प-सम
सुख का राहित्य है वह
सार-शून्य शब्द-झुण्ड...।
साहित्य शब्द ढ़लता-सा !
‘‘हित से जो युक्त—समन्वित होता है
वह सहित माना है
और
सहित का भाव ही
साहित्य बाना है,
अर्थ यह हुआ कि
जिसके आवलोकन से
सुख का समुद्भव-सम्पादन हो
सही साहित्य वही है
अन्यथा,
सुरभि से विरहित पुष्प-सम
सुख का राहित्य है वह
सार-शून्य शब्द-झुण्ड...।
(पृष्ठ 110-111)
‘मूक माटी’ को सन्त-कवि ने चार खण्डों में विभक्त किया है :
खण्डः 1 संकर नहीं : वर्ण-लाभ
खण्ड: 2 शब्द सो बोध नहीं : बोध सो सोध नहीं
खण्ड: 3 पुण्य का पालन : पाप-प्रक्षालन
खण्ड: 4 अग्नि की परीक्षा : चाँदी-सी राख
पहला खण्ड माटी की उस प्राथमिक दशा के परिशोधन की प्रक्रिया को व्यक्त करता है जहाँ वह पिण्ड रूप में कंकर-कणों से मिली जुली अवस्था में है। कुम्भकार की कल्पना में माटी का मंगल-घट अवतरित हुआ है। कुम्भकार माटी को मंगल-घट का जो सार्थक रूप देना चाहता है उसके लिए पहले यह आवश्यक है कि माटी को खोद कर, उसे कूट-छान कर, उसमें से कंकरों को हटा दिया जाए। माटी जो अभी वर्ण-संकर है, क्योंकि उसकी प्रकृति के विपरीत बेमेल तत्त्व कंकर उसमें आ मिले हैं। वह अपना मौलिक वर्णलाभ तभी प्राप्त करेगी जब वह मृदु माटी के रूप में अपनी शुद्ध दशा प्राप्त करे :
खण्डः 1 संकर नहीं : वर्ण-लाभ
खण्ड: 2 शब्द सो बोध नहीं : बोध सो सोध नहीं
खण्ड: 3 पुण्य का पालन : पाप-प्रक्षालन
खण्ड: 4 अग्नि की परीक्षा : चाँदी-सी राख
पहला खण्ड माटी की उस प्राथमिक दशा के परिशोधन की प्रक्रिया को व्यक्त करता है जहाँ वह पिण्ड रूप में कंकर-कणों से मिली जुली अवस्था में है। कुम्भकार की कल्पना में माटी का मंगल-घट अवतरित हुआ है। कुम्भकार माटी को मंगल-घट का जो सार्थक रूप देना चाहता है उसके लिए पहले यह आवश्यक है कि माटी को खोद कर, उसे कूट-छान कर, उसमें से कंकरों को हटा दिया जाए। माटी जो अभी वर्ण-संकर है, क्योंकि उसकी प्रकृति के विपरीत बेमेल तत्त्व कंकर उसमें आ मिले हैं। वह अपना मौलिक वर्णलाभ तभी प्राप्त करेगी जब वह मृदु माटी के रूप में अपनी शुद्ध दशा प्राप्त करे :
इस प्रसंग में
वर्ण का आशय/न ही रंग से है/न ही अंग से
वरन्/चाल-चरण, ढंग से है।
यानी !
जिसे अपनाया है
उस/जिसने अपनाया है
उसके अनुरूप
अपने गुण-धर्म—
...रूप-स्वरूप को
परिवर्तित करना होगा
वरना
वर्ण-संकर दोष को
...वरना होगा !...
केवल/ वर्ण-रंग की अपेक्षा
गाय का क्षीर भी धवल है/आक का क्षीर भी धवल है
दोनों ऊपर से विमल हैं।
परन्तु
परस्पर उन्हें मिलते ही/विकार उत्पन्य होता है,
क्षीर फट जाता है/पीर बन जाता है वह !
नीर का क्षीर बनना ही/ वर्ण-लाभ है, वरदान है।
और
क्षीर का फट जाना ही/ वर्ण-संकर है/ अभिशाप है।
वर्ण का आशय/न ही रंग से है/न ही अंग से
वरन्/चाल-चरण, ढंग से है।
यानी !
जिसे अपनाया है
उस/जिसने अपनाया है
उसके अनुरूप
अपने गुण-धर्म—
...रूप-स्वरूप को
परिवर्तित करना होगा
वरना
वर्ण-संकर दोष को
...वरना होगा !...
केवल/ वर्ण-रंग की अपेक्षा
गाय का क्षीर भी धवल है/आक का क्षीर भी धवल है
दोनों ऊपर से विमल हैं।
परन्तु
परस्पर उन्हें मिलते ही/विकार उत्पन्य होता है,
क्षीर फट जाता है/पीर बन जाता है वह !
नीर का क्षीर बनना ही/ वर्ण-लाभ है, वरदान है।
और
क्षीर का फट जाना ही/ वर्ण-संकर है/ अभिशाप है।
(पृष्ठ 47-49)
खण्ड दो—शब्द सो बोध नहीं : बोध सो शोध नहीं
लो, अब शिल्पी/ कुंकुम-सम माटी में
मात्रानुकूल मिलता है/ छना निर्मल-जल।
नूतन प्राण फूक रहा है/माटी के जीवन में।
करुणामय कण-कण में,....
माटी के प्राणों में जा, पानी ने वहाँ/नव-प्राण पाये हैं
ज्ञानी के पदों में जा/अज्ञानी ने जहाँ/नव-ज्ञान पाया है।
लो, अब शिल्पी/ कुंकुम-सम माटी में
मात्रानुकूल मिलता है/ छना निर्मल-जल।
नूतन प्राण फूक रहा है/माटी के जीवन में।
करुणामय कण-कण में,....
माटी के प्राणों में जा, पानी ने वहाँ/नव-प्राण पाये हैं
ज्ञानी के पदों में जा/अज्ञानी ने जहाँ/नव-ज्ञान पाया है।
(पृष्ठ 89)
माटी को खोदने की प्रक्रिया में कुम्भकार की कुदाली एक काँटे के माथे पर जा लगती है, उसका सिर फट जाता है। वह बदला लेने की सोचता है कि कुम्भकार को अपनी असावधानी पर ग्लानि होती है। उसके उद्गार हैं :
खंम्मामि, खमंतु मे—
खंम्मामि, खमंतु मे—
क्षमा करता हूँ सबको,/ क्षमा चाहता हूँ सबसे,
सबसे सदा-सहज बस/मैत्री रहे मेरी....
यहाँ कोई भी तो नहीं है/संसार-भर में मेरा वैरी !
सबसे सदा-सहज बस/मैत्री रहे मेरी....
यहाँ कोई भी तो नहीं है/संसार-भर में मेरा वैरी !
(पृष्ठ 105)
इस भावना का प्रभाव प्रतिलक्षित हुआ—
क्रोध भाव का शमन हो रहा है...
प्रतिशोध भाव का वमन हो रहा है...
पुण्य-निधि का प्रतिनिधि बना
बोध-भाव का आगमन हो रहा है
क्रोध भाव का शमन हो रहा है...
प्रतिशोध भाव का वमन हो रहा है...
पुण्य-निधि का प्रतिनिधि बना
बोध-भाव का आगमन हो रहा है
(पृष्ठ 106)
× × × × × ×
बोध के सिंचन बिना/शब्दों के पौधे ये/ कभी लहलहाते नहीं....
शब्दों के पौधों पर /सुगन्ध मकरन्द-भरे
बोध के फूल कभी महकते नहीं...
बोध का फूल जब/ढलता-बदलता, जिसमें,
वह पक्व फल ही तो/शोध कहलाता है।
बोध में अकुलता पलती है
सोध में निराकुलता फलती है,
फूल से नहीं, फल से /तृप्ति का अनुभव होता है।
शब्दों के पौधों पर /सुगन्ध मकरन्द-भरे
बोध के फूल कभी महकते नहीं...
बोध का फूल जब/ढलता-बदलता, जिसमें,
वह पक्व फल ही तो/शोध कहलाता है।
बोध में अकुलता पलती है
सोध में निराकुलता फलती है,
फूल से नहीं, फल से /तृप्ति का अनुभव होता है।
(पृष्ठ 106-107)
इस दूसरे खण्ड में सन्त-कवि ने साहित्य-बोध को अनेक आयामों में अंकित किया है। यहाँ नव रसों को परिभाषित किया है। संगीत की अन्तरंग प्रकृति का प्रतिपादन है। श्रृंगार रस की नितान्त मौलिक व्याख्या है। ऋतुओं के वर्णन में कविता का चमत्कार मोहक है। तत्त्व-दर्शन तो, जैसा मैं कह चुका हूँ, अनायास ही पद-पद पर उभर आता है।
‘उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-युक्तं सत्’ सूत्र का व्यावहारिक भाषा में चमत्कारी अनुवाद किया है :
‘उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-युक्तं सत्’ सूत्र का व्यावहारिक भाषा में चमत्कारी अनुवाद किया है :
आना, जाना, लगा हुआ है
आना यानी जनन-उत्पाद है,
जाना यानी मरण-व्यय है
लगा हुआ यानी स्थिर-ध्रौव्य है
और
है यानी चिर-सत्
यही सत्य है, यही तथ्य....
आना यानी जनन-उत्पाद है,
जाना यानी मरण-व्यय है
लगा हुआ यानी स्थिर-ध्रौव्य है
और
है यानी चिर-सत्
यही सत्य है, यही तथ्य....
(पृष्ठ 188)
भाव यह है कि उच्चारण मात्र ‘शब्द’ है, शब्द का सम्पूर्ण अर्थ समझना ‘बोध’ है, और इस बोध को अनुभूति में, आचरण में उतारना ‘शोध’ है।
खण्ड तीन-पुण्य का पालन : पाप-प्रक्षालन
मन, वचन काय की निर्मलता से, शुभ कार्यों के सम्पादन से, लोक-कल्याण की कामना से, पुण्य उपार्जित होता है। क्रोध, मन, माया, लोभ से पाप फलित होता है।
यह बात निराली है, कि
मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है
कारण कि
मुक्ता का उपादान जल है,
यानी-जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है,
तथापि
इस विषय पर विचार करने से/विदित होता है कि
इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है।
जल को मुक्ता के रूप में ढालने में
शुक्तिका-सीप कारण है
और/सीप स्वयं धरती का अंश है।
स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर
सागर में प्रेषित किया है।
जल को जड़त्व से मुक्त कर/मुक्ता-फल बनाना है,
पतन के गर्त से निकाल कर/उत्तुंग-उत्थान पर धरना,
धृति-धारिणी धरा का ध्येय है।
यही दया-धर्म है
यही जिया कर्म है।
मौलिक मुक्ताओं का निधान सागर भी है
कारण कि
मुक्ता का उपादान जल है,
यानी-जल ही मुक्ता का रूप धारण करता है,
तथापि
इस विषय पर विचार करने से/विदित होता है कि
इस कार्य में धरती का ही प्रमुख हाथ है।
जल को मुक्ता के रूप में ढालने में
शुक्तिका-सीप कारण है
और/सीप स्वयं धरती का अंश है।
स्वयं धरती ने सीप को प्रशिक्षित कर
सागर में प्रेषित किया है।
जल को जड़त्व से मुक्त कर/मुक्ता-फल बनाना है,
पतन के गर्त से निकाल कर/उत्तुंग-उत्थान पर धरना,
धृति-धारिणी धरा का ध्येय है।
यही दया-धर्म है
यही जिया कर्म है।
(पृष्ठ 192-193)
इस तीसरे खण्ड में कुम्भकार ने माटी की विकास-कथा के माध्यम से पुण्य-कर्म के सम्पादन से उपजी श्रेयस्कर उपलब्धि का चित्रण किया है। मेघ से मेघ-मुक्ता का अवतार। मुक्ता का वर्षण होता है अपक्व कुम्भों पर, कुम्भकार के प्रांगण में। मोतियों की वर्षा का समाचार पहुँचा राजा के पास। मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला राजा की मण्डली को।...नीचे झुकी मण्डली राशि भरने को ज्यों ही, गगन में गुरु गम्भीर गर्जना—अनर्थ, अनर्थ, अनर्थ ! पाप...पाप...पाप !
राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मन्त्र शक्ति द्वारा उसे कीतिल किया गया है। अन्त में कुम्भकार ने यह सोच कर कि मुक्ता-राशि पर वास्तव में राजा का ही अधिकार है, उसे समर्पित कर दिया।
धरती की कीर्ति देख कर सागर को क्षोभ/सागर के क्षोभ का प्रतिपक्षी बड़वानल/ तीन घन बादलों की उमड़न—कृष्ण, नील, कपोत लेश्याओं के प्रतीक/सागर द्वारा राहु का आह्वान/सूर्यग्रहण/इन्द्र द्वारा मेघों पर बज्रप्रहार ओलों की वर्षा, प्रलयंकर दृश्य।
राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मन्त्र शक्ति द्वारा उसे कीतिल किया गया है। अन्त में कुम्भकार ने यह सोच कर कि मुक्ता-राशि पर वास्तव में राजा का ही अधिकार है, उसे समर्पित कर दिया।
धरती की कीर्ति देख कर सागर को क्षोभ/सागर के क्षोभ का प्रतिपक्षी बड़वानल/ तीन घन बादलों की उमड़न—कृष्ण, नील, कपोत लेश्याओं के प्रतीक/सागर द्वारा राहु का आह्वान/सूर्यग्रहण/इन्द्र द्वारा मेघों पर बज्रप्रहार ओलों की वर्षा, प्रलयंकर दृश्य।
ऊपर अणु की शक्ति काम कर रही है
तो इधर...नीचे/मनु की शक्ति विद्यमान !
एक मारक है, एक तारक
एक विज्ञान है/जिसकी अजीविका तर्कणा है,
एक आस्था है/जिसे आजीविका की चिन्ता नहीं
तो इधर...नीचे/मनु की शक्ति विद्यमान !
एक मारक है, एक तारक
एक विज्ञान है/जिसकी अजीविका तर्कणा है,
एक आस्था है/जिसे आजीविका की चिन्ता नहीं
(पृष्ठ 249)
× × × × × × × × ×
जल और ज्वलनशील अनल में
अन्तर शेष रहता ही नहीं/साधक की अन्तर दृष्टि में।
निरन्तर साधना की यात्रा/भेद से अभेद की ओर
वेद से अवेद की ओर/बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए
अन्तर शेष रहता ही नहीं/साधक की अन्तर दृष्टि में।
निरन्तर साधना की यात्रा/भेद से अभेद की ओर
वेद से अवेद की ओर/बढ़ती है, बढ़ना ही चाहिए
(पृष्ठ 267)
खण्ड चार—अग्नि की परीक्षा : चाँदी-सी राख कुम्भकार ने घट को रूपाकार दे दिया है, अब उसे अवा में तपाने की तैयारी है। पूरी प्रक्रिया काव्य-बद्ध है। अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं के बीच बबूल की लकड़ी अपनी व्यथा कहती है। अवे मे लकड़ियाँ जलती हैं, बुझती हैं, बराबर कुम्भकार उन्हें प्रज्वलित करता है। अपक्व कुम्भ कहता है अग्नि से :
मेरे दोषों को जलाना ही/मुझे जिलाना है।
स्व-पर दोषों को जलाना/परम-धर्म माना है सन्तों ने।
दोष अजीव हैं, /नैमित्तिक हैं
बाहर से आगत हैं कथंचित्;
गुण जीवगत हैं,/गुण का स्वागत है।
तुम्हें पर्मार्थ मिलेगा इस कार्य से,
इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे,
मुझमें जल-धारण करने की शक्ति है
जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है,
उसकी पूरी अभिव्यक्ति में/ तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है।
स्व-पर दोषों को जलाना/परम-धर्म माना है सन्तों ने।
दोष अजीव हैं, /नैमित्तिक हैं
बाहर से आगत हैं कथंचित्;
गुण जीवगत हैं,/गुण का स्वागत है।
तुम्हें पर्मार्थ मिलेगा इस कार्य से,
इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे,
मुझमें जल-धारण करने की शक्ति है
जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है,
उसकी पूरी अभिव्यक्ति में/ तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है।
(पृष्ठ 277)
चौथे खण्ड का फलक इतना विस्तृत है और कथा-प्रसंग इतने अधिक हैं कि उनका सार-संक्षेप देना भी कठिन है। अवा में कुम्भ कई दिन तक तपा है। अवे के पास आता है कुम्भकार :
‘कुम्भ की कुशलता सो अपनी कुशलता’
यूँ कहता हुआ कुम्भकार/सोल्लास स्वागत करता है अवा का,
और/रेतिल राख की राशि को,/ जो अवा की छाती पर थी
हाथों में फावड़ा ले, हटाता है।
ज्यों-ज्यों राख हटती जाती,
त्यों-त्यों कुम्भकार का कुतूहल
बढ़ता जाता है, कि
कब दिखे वह कुशल कुम्भ....।
यूँ कहता हुआ कुम्भकार/सोल्लास स्वागत करता है अवा का,
और/रेतिल राख की राशि को,/ जो अवा की छाती पर थी
हाथों में फावड़ा ले, हटाता है।
ज्यों-ज्यों राख हटती जाती,
त्यों-त्यों कुम्भकार का कुतूहल
बढ़ता जाता है, कि
कब दिखे वह कुशल कुम्भ....।
और, पके-तपे कुम्भ को निकालता है बाहर, सोल्लास। इसी कुम्भ को कुम्भकार ने दिया है श्रद्धालु नगर-सेठ के सेवक के हाथों कि इसमें भरे जल से आहारदान के लिए पधारे गुरु का पाद-प्रक्षालन हो, तृषा तृप्त हो। ले जाने से पहले सात बार बजाता है सेवक और सात स्वर उसमें से ध्वनित होते हैं, जिनका अर्थ कवि के मन में इस प्रकार प्रतिध्वनित होता है :
सा...रे...ग..म....यानी (सारे गम)
सभी प्रकार के दुःख
प...ध...यानी पद-स्वभाव
और/नि यानी नहीं—
दुःख आत्मा का स्वभाव—धर्म नहीं हो सकता,
मोह-कर्म से प्रभावित आत्मा का
विभाव परिणमन मात्र है वह।
सभी प्रकार के दुःख
प...ध...यानी पद-स्वभाव
और/नि यानी नहीं—
दुःख आत्मा का स्वभाव—धर्म नहीं हो सकता,
मोह-कर्म से प्रभावित आत्मा का
विभाव परिणमन मात्र है वह।
(पृष्ठ 305)
इसी प्रसंग में मृदंग के स्वर भी गुंजरित होते हैं :
धा..धिन्...धिन्..धा..
धा..धिन्...धिन्..धा..
वेतन-भिन्ना, चेतन-भिन्ना
ता..तिन..तिन...ता
ता..तिन..तिन...ता
का तन..चिन्ता, का तन..चिन्ता ?
धा..धिन्...धिन्..धा..
धा..धिन्...धिन्..धा..
वेतन-भिन्ना, चेतन-भिन्ना
ता..तिन..तिन...ता
ता..तिन..तिन...ता
का तन..चिन्ता, का तन..चिन्ता ?
(पृष्ठ 306)
इस खण्ड में साधु की आहार दान की प्रक्रिया साविवरण उजागर हुई है। भक्तों की भावना, आहार देने या न दे सकने का हर्ष-विषाद, साधु की दृष्टि, धर्मोपदेश का सार और आहार-दान के उपरान्त सेठ का अनमने भाव से घर लौटना, सम्भवतः इसलिए कि सेठ को जीवन का गन्तव्य दिखाई दे गया है, किन्तु वह अभी बन्धन-मुक्त नहीं हो सकता :
सन्त समागम की यही तो सार्थकता है
संसार का अन्त दिखने लगता है,
समागम करने वाला भले ही
तुरन्त सन्त-संयत/बने या न बने
इसमें कोई नियम नहीं है,
किन्तु वह सन्तोषी अवश्य बनता है।
सही दिशा का प्रसाद ही
सही दशा का प्रसाद है।
संसार का अन्त दिखने लगता है,
समागम करने वाला भले ही
तुरन्त सन्त-संयत/बने या न बने
इसमें कोई नियम नहीं है,
किन्तु वह सन्तोषी अवश्य बनता है।
सही दिशा का प्रसाद ही
सही दशा का प्रसाद है।
(पृष्ठ 345)
प्रसंगों का, बात में से बात की उद्भावना का, तत्त्व-चिन्तन के ऊँचे छोरों को देखने-सुनने का, और लौकिक तथा पारलौकिक जिज्ञासाओ एवं अन्वेषणों का एक विचित्र छवि-घर है यह चतुर्थ खण्ड। यहाँ पूजा उपासना के उपकरण सजीव वार्तालाप में निमग्न हो जाते हैं। मानवीय भावनाएँ गुण और अवगुण, इनके माध्यम से अभिव्यक्ति पाते हैं। यह अद्भुत नाटकीयता, अतिशयता और प्रसंगों के पूर्वापर सम्बन्धों का विखराव समीक्षक के लिए असुविधाजनक हो सकते हैं, किन्तु काव्य को प्रासंगिक बनाने की दृष्टि से इनकी परिकल्पना साहसिक, सार्थक और आधुनिक परिदृश्य के अनुकूल है। यह खण्ड अपने आप में एक खण्ड काव्य है। यह पूरा-का-पूरा उद्धृत करने योग्य है। कठिनाई यह है कि थोड़े से उद्धरण देना कृति के प्रति न्याय नहीं। जो छूटा है वह अपेक्षाकृत विशाल है, महत्त्वपूर्ण हैं। अस्तु। देखें कथा-प्रसंग को : स्वर्णकलश उद्विग्न और उत्तप्त है कि कथानायक ने उसकी उपेक्षा करके मिट्टी के घड़े को आदर क्यों दिया है। इस अपमान का बदला लेने के लिए स्वर्णकलश एक आतंकवादी दल आहूत करता है जो सक्रिय होकर परिवार में त्राहि-त्राहि मचा देता है। उसके क्या कारनामें हैं, किन विपत्तियों में से सेठ अपने परिवार की रक्षा स्वयं और सहयोगी प्राकृतिक शक्तियों तथा मनु्ष्येतर प्रणियों—गजदल और नाग नागनियों—की सहायता से कर पाता है, मँझधार में डूबती नाव से किस प्रकार सबकी प्राण-रक्षा होती है, किस प्रकार सेठ का क्षमाभाव आतंकवादियों का हृदय परिवर्तन करता है, इस सबका विवरण उपन्यास से कम रोचक नहीं। कविता का रसास्वाद तो भरपूर है ही। हम माने तो मान सकते हैं कि ‘स्वर्णकलश’ और आतंकवाद आज के जीवन के ताज़े सन्दर्भ हैं। समाधान आज के प्रसंगों के अनुरूप आधुनिक समाज-व्यवस्था के विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सीधे सपाट ढंग से नहीं, काव्य की लक्षणा और व्यंजना पद्धति से। विचित्र बात यह है कि सामाजिक दायित्व-बोध हमें प्राप्त होता है एक मत्कुण के माध्यम से :
...खेद है कि
लोभी पापी मानव
पाणिग्रहण को भी
प्राण-ग्रहण का रूप देते हैं।
प्रायः अनुचित रूप से
सेवकों से सेवा लेते/और
वेतन का वितरण भी अनुचित ही।
ये अपने को बताते/मनु की सन्तान !
महामना मानव !
देने का नाम सुनते ही
इनके उदार हाथों में
पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं,
फिर भी, एकाध बूँद के रूप में
जो कुछ दिया जाता/या देना पड़ता
वह दुर्भावना के साथ ही।
जिसे पाने वाले पचा न पाते सही
अन्यथा
हमारा रूधिर लाल होकर भी
इतना दुर्गन्ध क्यों ?
लोभी पापी मानव
पाणिग्रहण को भी
प्राण-ग्रहण का रूप देते हैं।
प्रायः अनुचित रूप से
सेवकों से सेवा लेते/और
वेतन का वितरण भी अनुचित ही।
ये अपने को बताते/मनु की सन्तान !
महामना मानव !
देने का नाम सुनते ही
इनके उदार हाथों में
पक्षाघात के लक्षण दिखने लगते हैं,
फिर भी, एकाध बूँद के रूप में
जो कुछ दिया जाता/या देना पड़ता
वह दुर्भावना के साथ ही।
जिसे पाने वाले पचा न पाते सही
अन्यथा
हमारा रूधिर लाल होकर भी
इतना दुर्गन्ध क्यों ?
(पृष्ठ 386-87)
और सेठ से मत्कुण कहता है :
सूखा प्रलोभन मत दिया करो
स्वाश्रित जीवन जिया करो,
कपटता की पटुता को
जलांजलि दो !
गुरुता की जनिका लघुता को
श्रद्धांजलि दो !
शालीनता की विशालता में
आकाश समा जाय
और
जीवन उदारता का उदाहरण बने !
अकारण ही—
पर के दुःख का सदा हरण हो !
सूखा प्रलोभन मत दिया करो
स्वाश्रित जीवन जिया करो,
कपटता की पटुता को
जलांजलि दो !
गुरुता की जनिका लघुता को
श्रद्धांजलि दो !
शालीनता की विशालता में
आकाश समा जाय
और
जीवन उदारता का उदाहरण बने !
अकारण ही—
पर के दुःख का सदा हरण हो !
(पृष्ठ 387-88)
और अन्त में पाषाण-फलक पर आसीन नीराग साधु की वन्दना के उपरान्त स्वयं आतंकवाद कहता है :
हे स्वामिन् ! समग्र संसार ही/दुःख से भरपूर है !
यहाँ सुख है, पर वैषयिक/और वह भी क्षणिक !
यह...तो...अनुभूत हुआ हमें,
परन्तु
अक्षय सुख पर/विश्वास नहीं हो रहा है;
हाँ, हाँ !! यदि/अविनश्वर सुख पाने के बाद
आप स्वयं/उस सुख को हमें दिखा सको/या
उस विषय में/अपना अनुभव बता सको...तो
सम्भव है/हम भी विश्वस्त हो
आप-जैसी साधना को
जीवन में अपना सकें।..
‘तुम्हारी भावना पूरी हो’/ऐसे वचन दो हमें,
बड़ी कृपा होगी हम पर।
यहाँ सुख है, पर वैषयिक/और वह भी क्षणिक !
यह...तो...अनुभूत हुआ हमें,
परन्तु
अक्षय सुख पर/विश्वास नहीं हो रहा है;
हाँ, हाँ !! यदि/अविनश्वर सुख पाने के बाद
आप स्वयं/उस सुख को हमें दिखा सको/या
उस विषय में/अपना अनुभव बता सको...तो
सम्भव है/हम भी विश्वस्त हो
आप-जैसी साधना को
जीवन में अपना सकें।..
‘तुम्हारी भावना पूरी हो’/ऐसे वचन दो हमें,
बड़ी कृपा होगी हम पर।
(पृष्ठ 484-85)
गुरु तो प्रवचन ही दे सकते हैं, ‘वचन’नहीं। आत्मा का उद्धार तो अपने ही पुरुषार्थ से हो सकता है और अविनश्वर सुख वचनों से बताया नहीं जा सकता। वह तो साधना से प्राप्त आत्मोपलब्धि है। साधु की देशना है :
बन्धन रूप तन/मन और वचन का
आमूल मिट जाना ही/मोक्ष है।
इसी मोक्ष की शुद्ध-दशा में/ अविनश्वर सुख होता है।
जिसे
प्राप्त होने के बाद,
यहाँ
संसार में आना कैसे सम्भव है,
तुम ही बताओ
× × × ×
विश्वास को अनुभूति मिलेगी
अवश्य मिलेगी/मगर
मार्ग में नहीं, मंजिल पर।
और
महामौन में डूबते हुए सन्त...
और, महौल को अनिमेष निहारती-सी
...मूक माटी।
आमूल मिट जाना ही/मोक्ष है।
इसी मोक्ष की शुद्ध-दशा में/ अविनश्वर सुख होता है।
जिसे
प्राप्त होने के बाद,
यहाँ
संसार में आना कैसे सम्भव है,
तुम ही बताओ
× × × ×
विश्वास को अनुभूति मिलेगी
अवश्य मिलेगी/मगर
मार्ग में नहीं, मंजिल पर।
और
महामौन में डूबते हुए सन्त...
और, महौल को अनिमेष निहारती-सी
...मूक माटी।
(पृष्ठ 488)
ये कुछ संकेत हैं ‘मूक माटी’ की कथावस्तु के, उसके काव्य की गरिमा, कथ्य के आध्यात्मिक आयामों, दर्शन और चिन्तन के प्रेरणादायक स्फुरणों के।
इन सब के अतिरिक्त और बहुत कुछ प्रासंगिक और आनुषंगिक है इस महाकाव्य में, यथा लोकजीवन के रचे-पचे मुहावरे, बीजाक्षरों के चमत्कार, मन्त्रविद्या की आधार-भित्ति, आयुर्वेद के प्रयोग, अंकों का चमत्कार, और आधुनिक जीवन में विज्ञान से उपजी कतिपय नयी अवधारणाएँ जो ‘स्टार-वार’ तक पहुँचती हैं।
यह कृति अधिक परिमाण में काव्य है या अध्यात्म, कहना कठिन है। लेकिन निश्चय ही यह है आधुनिक जीवन का अभिनव शास्त्र। और, जिस प्रकार शास्त्र का श्रद्धापूर्वक स्वाध्याय करना होता है, गुरु से जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करना होता है, उसी प्रकार इसका अध्ययन और मनन अद्भुत सुख और सन्तोष देगा, ऐसा विश्वास है।
यह भूमिका नहीं, आमुख और प्राक्कथन नहीं। यह प्रस्तवन है, संस्तुवन है—तपस्वी आचार्य सन्त-कवि विद्यासागर जी का, जिनकी प्रज्ञा और काव्य-प्रतिभा से यह कल्पवृक्ष उपजा है।
णमो णाणगुरूणं
जिन आत्म-द्रष्टा से
दर्शन मिला
जिन मन्त्र-स्रष्टा से
मन्त्र मिला
जिनने पद दिया
पथ दिया
पाथेय भी दिया
जिनके कोमल कर-पल्लवों से
यह जीवन पोषित हुआ
मोह का प्रताप शोषित हुआ
उन गारव-रहित
गुण के आगर गुरुवर
श्री ज्ञानसागर जी के
सुखद कर-कमलों में
परोक्षरूप से
मूक माटी सृजन का
समर्पण करता हुआ
जिन आत्म-द्रष्टा से
दर्शन मिला
जिन मन्त्र-स्रष्टा से
मन्त्र मिला
जिनने पद दिया
पथ दिया
पाथेय भी दिया
जिनके कोमल कर-पल्लवों से
यह जीवन पोषित हुआ
मोह का प्रताप शोषित हुआ
उन गारव-रहित
गुण के आगर गुरुवर
श्री ज्ञानसागर जी के
सुखद कर-कमलों में
परोक्षरूप से
मूक माटी सृजन का
समर्पण करता हुआ
मानस-तरंग
सामान्यतः जो है, उसका अभाव नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं, उसका उत्पाद भी सम्भव नहीं। इस तथ्य का स्वागत केवल दर्शन ने ही नहीं, नूतन भौतिक युग ने भी किया है।
यद्यपि प्रति वस्तु की स्वभावभूत-सृजनशीलता एवं परिणमनशीलता से वस्तु का त्रिकाल-जीवन सिद्ध होता है, तथापि इस अपार संसार का सृजक-स्रष्टा कोई असाधारण बलशाली पुरूष है, और वह ईश्वर को छोड़कर कौन हो सकता है ? इस मान्यता का समर्थन प्रायः सभी दर्शनकार करते हैं। वे कार्य-कारण व्यवस्था से अपरिचित हैं।
किसी भी ‘कार्य का कर्ता कौन है और कारण कौन ?’ इस विषय का जब तक भेद नहीं खुलता, तब तक ही यह संसारी जीव मोही, अपने से भिन्नभूत अनुकूल पदार्थों के सम्पादन-संरक्षण में और प्रतिकूलताओं के परिहार में दिनरात तत्पर रहता है।
हाँ, तो चेतन-सम्बन्धी कार्य हो या अचेतन सम्बन्धी, बिना किसी कारण, उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि कार्य कारण के अनुरूप ही हुआ करता है। जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल पाते है, विपरीत नहीं।
वैसे मुख्यरूप से कारण के दो रूप हैं—एक उपादान और एक निमित्त—(उपादान को अन्तरंग कारण और निमित्त को बाह्य-कारण कह सकते हैं।) उपादान कारण वह है, जो कार्य के रूप में ढलता है; और उसके ढलने में जो सहयोगी होता है वह है निमित्त। जैसे माटी का लोंदा कुम्भकार के सहयोग से कुम्भ के रूप में बदलता है।
उपरिल उदाहरण सूक्ष्म रूप से देखने पर इसमें केवल उपादान ही नहीं, अपितु निमित्त की भी अपनी मौलिकताएँ समने आती हैं। यहाँ पर निमित्त-कारण के रूप में कार्यरत कुम्भकार के शिवा और भी कई निमित्त हैं—आलोक, चक्र, चक्र-भ्रमण हेतु समुचित दण्ड, डोर और धरती में गड़ी निष्कम्प-कील आदि-आदि।
इन निमित्त कारणों में कुछ उदासीन हैं, कुछ प्रेरक। ऐसी स्थिति में निमित्त कारणों के प्रति अनास्था रखनेवालों से यह लेखनी यही पूछती है कि :
-क्या आलोक के अभाव में कुशल कुम्भकार भी कुम्भ का निर्माण कर सकता है ?
-क्या चक्र के बिना माटी का लोंदा कुम्भ के रूप में ढल सकता है ?
-क्या बिना दण्ड के चक्र का भ्रमण सम्भव है ?
-क्या कील का आधार लिये बिना चक्र का भ्रमण सम्भव है ?
क्या सबके आधारभूत धरती के अभाव में वह सब कुछ घट सकता है ?
-क्या कील और आलोक के समान कुम्भकार भी उदासीन है ?
-क्या कुम्भकार के करों में कुम्भकार आये बिना स्पर्श-मात्र से माटी की लोंदा कुम्भ का रूप धारण कर सकता है ?
-कुम्भकार का उपयोग, कुम्भकार हुए बिना, कुम्भकार के करों में कुम्भकार आ सकता है ?
-क्या बिना इच्छा भी कुम्भकार अपने उपयोग को कुम्भकार दे सकता है ?
-क्या कुम्भ बनाने की इच्छा निरुद्देश्य होती है ?
इन सब प्रश्नों का समाधान ‘नहीं’ इस शब्द के सिवा और कौन देता है ?
निमित्त की इस अनिवार्यता को देखकर ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना भी वस्तु-तत्त्व की स्वतन्त्र योग्यता को नकारना है और ईश्वर-पद की पूज्यता पर प्रश्न-चिह्न लगाना है।
तत्त्वखोजी, तत्त्वभोजी वर्ग में ही नहीं, ईश्वर के सही उपासकों में भी यह शंका जन्म ले सकती है कि सृष्टि-रचना से पूर्व ईश्वर का आवास कहाँ था ? वह शरीरातीत था या सशरीरी ?
अशरीरी होकर असीम सृष्टि की रचना करना तो दूर, सांसारिक छोटी-छोटी क्रिया भी नहीं की जा सकतीं। हाँ, ईश्वर मुक्तावस्था को छोड़ कर पुनः शरीर को धारण कर जागतिक-कार्य कर लेता है, ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि शरीर की प्राप्ति कर्मों पर, कर्मों का बन्धन शुभाशुभ विभाव-भावों पर आधारित है और ईश्वर इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है यह सर्व-सम्मत है।
विषय-कषायों को त्याग कर जितेन्द्रिय, जितकषाय और विजितमना हो जिसने पूरी आस्था के साथ आत्म-साधना की है और अपने में छुपी हुई ईश्वरीय शक्ति का उद्घाटन कर अविनश्वर सुख को प्राप्त किया है, वह ईश्वर अब संसार में अवतरित नहीं हो सकता है। दुग्ध में से घृत को निकालने के बाद घृत कभी दुग्ध के रूप में लौट सकता है क्या ?
ईश्वर को सशरीरी मानने रूप दूसरा विकल्प भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शरीर अपने आप में वह बन्धन है जो सब बन्धनों का मूल है। शरीर है तो संसार है, संसार में दुःख के सिवा और क्या है ? अतः ईश्वरत्व किसी भी दुःखरूप बन्धन को स्वीकार-सहन नहीं कर सकता है। वैसे ईश्वरत्व की उपलब्धि संसारदशा में सम्भव नहीं। हाँ, संसारी ईश्वर बन सकता है, साधना के बल पर, सांसारिक बन्धनों को तोड़ कर।
यह भी नहीं कहा जा सकता है कि विद्याओं, विक्रियाओं के बल पर, विद्याधरों और देवों के द्वारा भी मनोहर नगरादिकों दिशा की जब रचना की जाती है, तब सशरीरी ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना में क्या बाधा है ? क्योंकि देवादिकों में से निर्मित नगरादिक तात्कालिक होते हैं, न कि त्रैकालिक। यह भी सीमित होते हैं न कि विश्वव्यापक। और यहाँ परोपकार का प्रयोजन नहीं अपितु विषय-सुख के प्यासे मन की तुष्टि है। सही बात तो यह है कि विद्या-विक्रियाएँ भी पूर्व-कृत पुण्योदय के अनुरूप ही फलती हैं, अन्यथा नहीं।
जैनदर्शक सम्मत सकल परमात्मा भी, जो कर्म-पर्वतों के भेत्ता, विश्व-तत्त्वों के ज्ञाता और मोक्ष-मार्ग के नेता के रूप में स्वीकृत हैं, सशरीरी हैं। वह जैसे धर्मोपदेश देकर संसारी जीवों का उपकार करते हैं वैसे ही ईश्वर सृष्टि-रचना करके हमको सबको उपकृत करते हैं, ऐसा कहना भी युक्ति-युक्त नहीं है। क्योंकि प्रथम तो जैन-दर्शन ने सकल परमात्मा को भगवान् के रूप में औपचारिक स्वीकार किया है। यथार्थ में उन्हें स्नातक-मुनि की संज्ञा दी है और ऐसे ही वीतराग, यथाजात-मुनि निःस्वार्थ धर्मोपदेश देते हैं।
जिन-शासन के धर्मोपदेश को आधार बनाकर अपने मत की पुष्टि के लिए ईश्वर को विश्व-कर्मा के रूप में स्वीकारना ही ईश्वर को पक्षपात की मूर्ति, रागी-द्वेषी सिद्ध करना है। क्योंकि उनके कार्य कार्य-भूत संसारी जीव, कुछ निर्धन, कुछ धनी, कुछ निर्गुण, कुछ गुणी, कुछ दीन-हीन-दयनीय-पदाधीन, कुछ स्वतन्त्र-स्वाधीन-समृद्ध, कुछ नर, कुछ वानर-पशु-पक्षी, कुछ छली-कपटी-धूर्त हृदयशून्य, कुछ सुकृति पुण्यआत्मा, कुछ सुरूप-सुन्दर, कुछ कुरूप-विद्रूप आदि-आदि क्यों हैं ? इन सबको समान क्यों न बनाते वह ईश्वर ? अथवा अपने समान भगवान् बनाते सबको ? दीनदयाल दया-निधान का व्यक्तित्व ऐसा नहीं हो सकता। इस महान् दोष से ईश्वर को बचाने हेतु, यदि कहो, कि अपने-अपने किये हुए पुण्यापुण्य के अनुसार ही, संसारी जीवों को सुख-दुःख भोगने के लिए स्वर्ग-नरकादिकों में ईश्वर भेजता है, यह कहना भी अनुचित है क्योंकि जब इन जीवों की सारी विविधताएँ-विषमताएँ शुभाशुभ कर्मों की फलश्रुति हैं, फिर ईश्वर से क्या प्रयोजन रहा ? पुलिस के कारण नहीं; चोर चोरी के कारण जेल में पवेश पाता है, देवों के कारण नहीं, शील के कारण सीता का यश फैला है।
इस सन्दर्भ में एक बात और कहनी है कि ‘‘कुछ दर्शन, जैन-दर्शन को नास्तिक मानते हैं और प्रचार करते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे नास्तिक होते हैं। यह मान्यता उनकी दर्शन-विषयक अल्पज्ञता को ही सूचित करती है।’’
ज्ञात रहे, कि भ्रमण-संस्कृति के सम्पोषक जैन-दर्शन ने बड़ी आस्था के साथ ईश्वर को परम श्रद्धेय-पूज्य के रूप में स्वीकारा है, सृष्टि-कर्ता के रूप में नहीं। इसीलिए जैन-दर्शन, नास्तिक दर्शनों को सही दिशाबोध देनेवाला एक आदर्श आस्तिक दर्शन है। यथार्थ में ईश्वर को सृष्टि-कर्ता के रूप में स्वीकारना ही, उसे नकारना है, और यही नास्तिकता है, मिथ्या है। इस प्रासंगिक विषय की संपुष्टि महाभारत की हृदयस्थानीय ‘गीता’ के पंचम अध्याय की चौदहवीं और पन्द्रहवीं कारिकाओं से होती है—
यद्यपि प्रति वस्तु की स्वभावभूत-सृजनशीलता एवं परिणमनशीलता से वस्तु का त्रिकाल-जीवन सिद्ध होता है, तथापि इस अपार संसार का सृजक-स्रष्टा कोई असाधारण बलशाली पुरूष है, और वह ईश्वर को छोड़कर कौन हो सकता है ? इस मान्यता का समर्थन प्रायः सभी दर्शनकार करते हैं। वे कार्य-कारण व्यवस्था से अपरिचित हैं।
किसी भी ‘कार्य का कर्ता कौन है और कारण कौन ?’ इस विषय का जब तक भेद नहीं खुलता, तब तक ही यह संसारी जीव मोही, अपने से भिन्नभूत अनुकूल पदार्थों के सम्पादन-संरक्षण में और प्रतिकूलताओं के परिहार में दिनरात तत्पर रहता है।
हाँ, तो चेतन-सम्बन्धी कार्य हो या अचेतन सम्बन्धी, बिना किसी कारण, उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि कार्य कारण के अनुरूप ही हुआ करता है। जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फल पाते है, विपरीत नहीं।
वैसे मुख्यरूप से कारण के दो रूप हैं—एक उपादान और एक निमित्त—(उपादान को अन्तरंग कारण और निमित्त को बाह्य-कारण कह सकते हैं।) उपादान कारण वह है, जो कार्य के रूप में ढलता है; और उसके ढलने में जो सहयोगी होता है वह है निमित्त। जैसे माटी का लोंदा कुम्भकार के सहयोग से कुम्भ के रूप में बदलता है।
उपरिल उदाहरण सूक्ष्म रूप से देखने पर इसमें केवल उपादान ही नहीं, अपितु निमित्त की भी अपनी मौलिकताएँ समने आती हैं। यहाँ पर निमित्त-कारण के रूप में कार्यरत कुम्भकार के शिवा और भी कई निमित्त हैं—आलोक, चक्र, चक्र-भ्रमण हेतु समुचित दण्ड, डोर और धरती में गड़ी निष्कम्प-कील आदि-आदि।
इन निमित्त कारणों में कुछ उदासीन हैं, कुछ प्रेरक। ऐसी स्थिति में निमित्त कारणों के प्रति अनास्था रखनेवालों से यह लेखनी यही पूछती है कि :
-क्या आलोक के अभाव में कुशल कुम्भकार भी कुम्भ का निर्माण कर सकता है ?
-क्या चक्र के बिना माटी का लोंदा कुम्भ के रूप में ढल सकता है ?
-क्या बिना दण्ड के चक्र का भ्रमण सम्भव है ?
-क्या कील का आधार लिये बिना चक्र का भ्रमण सम्भव है ?
क्या सबके आधारभूत धरती के अभाव में वह सब कुछ घट सकता है ?
-क्या कील और आलोक के समान कुम्भकार भी उदासीन है ?
-क्या कुम्भकार के करों में कुम्भकार आये बिना स्पर्श-मात्र से माटी की लोंदा कुम्भ का रूप धारण कर सकता है ?
-कुम्भकार का उपयोग, कुम्भकार हुए बिना, कुम्भकार के करों में कुम्भकार आ सकता है ?
-क्या बिना इच्छा भी कुम्भकार अपने उपयोग को कुम्भकार दे सकता है ?
-क्या कुम्भ बनाने की इच्छा निरुद्देश्य होती है ?
इन सब प्रश्नों का समाधान ‘नहीं’ इस शब्द के सिवा और कौन देता है ?
निमित्त की इस अनिवार्यता को देखकर ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना भी वस्तु-तत्त्व की स्वतन्त्र योग्यता को नकारना है और ईश्वर-पद की पूज्यता पर प्रश्न-चिह्न लगाना है।
तत्त्वखोजी, तत्त्वभोजी वर्ग में ही नहीं, ईश्वर के सही उपासकों में भी यह शंका जन्म ले सकती है कि सृष्टि-रचना से पूर्व ईश्वर का आवास कहाँ था ? वह शरीरातीत था या सशरीरी ?
अशरीरी होकर असीम सृष्टि की रचना करना तो दूर, सांसारिक छोटी-छोटी क्रिया भी नहीं की जा सकतीं। हाँ, ईश्वर मुक्तावस्था को छोड़ कर पुनः शरीर को धारण कर जागतिक-कार्य कर लेता है, ऐसा कहना भी उचित नहीं, क्योंकि शरीर की प्राप्ति कर्मों पर, कर्मों का बन्धन शुभाशुभ विभाव-भावों पर आधारित है और ईश्वर इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है यह सर्व-सम्मत है।
विषय-कषायों को त्याग कर जितेन्द्रिय, जितकषाय और विजितमना हो जिसने पूरी आस्था के साथ आत्म-साधना की है और अपने में छुपी हुई ईश्वरीय शक्ति का उद्घाटन कर अविनश्वर सुख को प्राप्त किया है, वह ईश्वर अब संसार में अवतरित नहीं हो सकता है। दुग्ध में से घृत को निकालने के बाद घृत कभी दुग्ध के रूप में लौट सकता है क्या ?
ईश्वर को सशरीरी मानने रूप दूसरा विकल्प भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शरीर अपने आप में वह बन्धन है जो सब बन्धनों का मूल है। शरीर है तो संसार है, संसार में दुःख के सिवा और क्या है ? अतः ईश्वरत्व किसी भी दुःखरूप बन्धन को स्वीकार-सहन नहीं कर सकता है। वैसे ईश्वरत्व की उपलब्धि संसारदशा में सम्भव नहीं। हाँ, संसारी ईश्वर बन सकता है, साधना के बल पर, सांसारिक बन्धनों को तोड़ कर।
यह भी नहीं कहा जा सकता है कि विद्याओं, विक्रियाओं के बल पर, विद्याधरों और देवों के द्वारा भी मनोहर नगरादिकों दिशा की जब रचना की जाती है, तब सशरीरी ईश्वर के द्वारा सृष्टि की रचना में क्या बाधा है ? क्योंकि देवादिकों में से निर्मित नगरादिक तात्कालिक होते हैं, न कि त्रैकालिक। यह भी सीमित होते हैं न कि विश्वव्यापक। और यहाँ परोपकार का प्रयोजन नहीं अपितु विषय-सुख के प्यासे मन की तुष्टि है। सही बात तो यह है कि विद्या-विक्रियाएँ भी पूर्व-कृत पुण्योदय के अनुरूप ही फलती हैं, अन्यथा नहीं।
जैनदर्शक सम्मत सकल परमात्मा भी, जो कर्म-पर्वतों के भेत्ता, विश्व-तत्त्वों के ज्ञाता और मोक्ष-मार्ग के नेता के रूप में स्वीकृत हैं, सशरीरी हैं। वह जैसे धर्मोपदेश देकर संसारी जीवों का उपकार करते हैं वैसे ही ईश्वर सृष्टि-रचना करके हमको सबको उपकृत करते हैं, ऐसा कहना भी युक्ति-युक्त नहीं है। क्योंकि प्रथम तो जैन-दर्शन ने सकल परमात्मा को भगवान् के रूप में औपचारिक स्वीकार किया है। यथार्थ में उन्हें स्नातक-मुनि की संज्ञा दी है और ऐसे ही वीतराग, यथाजात-मुनि निःस्वार्थ धर्मोपदेश देते हैं।
जिन-शासन के धर्मोपदेश को आधार बनाकर अपने मत की पुष्टि के लिए ईश्वर को विश्व-कर्मा के रूप में स्वीकारना ही ईश्वर को पक्षपात की मूर्ति, रागी-द्वेषी सिद्ध करना है। क्योंकि उनके कार्य कार्य-भूत संसारी जीव, कुछ निर्धन, कुछ धनी, कुछ निर्गुण, कुछ गुणी, कुछ दीन-हीन-दयनीय-पदाधीन, कुछ स्वतन्त्र-स्वाधीन-समृद्ध, कुछ नर, कुछ वानर-पशु-पक्षी, कुछ छली-कपटी-धूर्त हृदयशून्य, कुछ सुकृति पुण्यआत्मा, कुछ सुरूप-सुन्दर, कुछ कुरूप-विद्रूप आदि-आदि क्यों हैं ? इन सबको समान क्यों न बनाते वह ईश्वर ? अथवा अपने समान भगवान् बनाते सबको ? दीनदयाल दया-निधान का व्यक्तित्व ऐसा नहीं हो सकता। इस महान् दोष से ईश्वर को बचाने हेतु, यदि कहो, कि अपने-अपने किये हुए पुण्यापुण्य के अनुसार ही, संसारी जीवों को सुख-दुःख भोगने के लिए स्वर्ग-नरकादिकों में ईश्वर भेजता है, यह कहना भी अनुचित है क्योंकि जब इन जीवों की सारी विविधताएँ-विषमताएँ शुभाशुभ कर्मों की फलश्रुति हैं, फिर ईश्वर से क्या प्रयोजन रहा ? पुलिस के कारण नहीं; चोर चोरी के कारण जेल में पवेश पाता है, देवों के कारण नहीं, शील के कारण सीता का यश फैला है।
इस सन्दर्भ में एक बात और कहनी है कि ‘‘कुछ दर्शन, जैन-दर्शन को नास्तिक मानते हैं और प्रचार करते हैं कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे नास्तिक होते हैं। यह मान्यता उनकी दर्शन-विषयक अल्पज्ञता को ही सूचित करती है।’’
ज्ञात रहे, कि भ्रमण-संस्कृति के सम्पोषक जैन-दर्शन ने बड़ी आस्था के साथ ईश्वर को परम श्रद्धेय-पूज्य के रूप में स्वीकारा है, सृष्टि-कर्ता के रूप में नहीं। इसीलिए जैन-दर्शन, नास्तिक दर्शनों को सही दिशाबोध देनेवाला एक आदर्श आस्तिक दर्शन है। यथार्थ में ईश्वर को सृष्टि-कर्ता के रूप में स्वीकारना ही, उसे नकारना है, और यही नास्तिकता है, मिथ्या है। इस प्रासंगिक विषय की संपुष्टि महाभारत की हृदयस्थानीय ‘गीता’ के पंचम अध्याय की चौदहवीं और पन्द्रहवीं कारिकाओं से होती है—
‘‘न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः।
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते।।
नाऽऽदत्ते कस्यचित् पापं न चेव सुकृतं विभुः।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।।’’
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते।।
नाऽऽदत्ते कस्यचित् पापं न चेव सुकृतं विभुः।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।।’’
प्रभु परमात्मा लोक के कर
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book